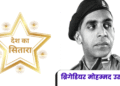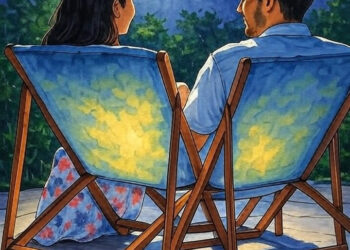श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें कई व्यावहारिक सीखें देता है. उनके जन्म के समय से ले कर उनकी मृत्यु तक के पूरे जीवन में इतने उतार-चढ़ाव हैं और उनके बीच जीवन को कैस जिया जा सकता है, यह बात मनमोहन हमें बताते ही नहीं हैं, बल्कि ख़ुद जी कर दिखाते हैं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, कृष्ण से जुड़े प्रतीकार्थों को समझा रही हैं, भावना प्रकाश.
आइए इस बार श्रीकृष्ण के जन्म की कथा से पहले एक दंतकथा सुनते हैं. एक काफ़िला कहीं जा रहा था. रात में पड़ाव डालने के लिए ऊंटों को बांधते समय देखा गया कि एक रस्सी कम है. काफ़िले के अनुभवी मुखिया ने एक समाधान निकाला. उसने अंतिम ऊंट को बैठाया, उसके गले में रस्सी बांधने का फिर उस रस्सी को खूंटे से बांधने का नाटक किया. ऊंट आराम से बैठ गया. सुबह जब सभी ऊंटो को खोला गया तो सब उठ खड़े हुए पर वो ऊंट उठ ही नहीं रही था. बड़ी कोशिश की गई पर सब बेकार. तभी उस अनुभवी मुखिया को रात की बात याद आई. उसने फिर रात की ही तरह ऊंट की रस्सी खोलने का नाटक किया. ऊंट तुरंत उठ खड़ा हुआ.
प्रहसन श्रीकृष्ण के जन्म का
अब आते हैं श्रीकृष्ण के जन्म की कथा पर. मध्य रात्रि का समय है. बिजली कड़क रही है और बादल गरज रहे हैं. बारिश अपनी पूरी क्षमता के साथ बरस रही है. नदियां उफ़ान पर हैं और पूरी सृष्टि में निविड़ अंधकार व्याप्त है. एक अन्यायी और क्रूर राजा के कारागृह में पति-पत्नी का एक जोड़ा बेड़ियों में जकड़ा थका हारा बैठा है. कारागृह के बाहर कड़ा पहरा है. स्त्री के गर्भ में एक जीव है. जोड़ा चिंतित और दुखी है, क्योंकि उनके अनेक बालक गर्भ की आयु पूरी करके जन्म लेते ही अन्यायी राजा की दृष्टि में पड़ गए और निर्ममता से समाप्त किए जा चुके हैं. तभी उस स्त्री के गर्भ में पल रहे बालक की गर्भ की आयु पूर्ण होती है और उस दिव्य बालक का जन्म हो जाता है. इस बार अचानक सब-कुछ बदल जाता है. उस दिव्य शिशु के आगमन से जोड़े के बंधन खुल जाते हैं. कारागृह के द्वार के ताले टूट जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं. उस जोड़े के निराश मन में आशा और समाधान की चेतना का संचार होता है और संघर्ष की राह प्रदीप्त होती है.
और तब उनमें साहस जागता है इस बार जन्में बालक की रक्षा का. और उसकी रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. वो स्त्री अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान करने को- इतने संघर्षों से पाए अपने पुत्र को अपने से दूर करने को राज़ी हो जाती है. पुरुष उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा देता है. यही नहीं, वो उस असह्य यातना को सहने को भी तैयार हो जाते हैं, जो अपने इस पुत्र को छिपा देने के अपराध में राजा द्वारा मिलेगी.
पुरुष उस बालक को अपने उस मित्र को सौंप आता है, जो अन्यायी और शोषक राजा के शोषण से पीड़ित प्रजा का एक जीता जागता उदाहरण है. वो मित्र एक ऐसे गांव का मुखिया है, जो अन्नदाता होने के बावजूद अनाज को और दुग्धदाता होने के बावजूद दूध, दही, मक्खन को तरस रहा है. वो अपना लगभग सारा उत्पादन शोषक राजा को कर के रूप में भेज दिए जाने को विवश है. यही नहीं, उन्हें तो सिंचाई के लिए वर्षा पाने हेतु भी अपनी बची-खुची तुच्छ संपदा इंद्रदेव की ‘पूजा’ में अर्पित कर देनी पड़ती है. वो शोषित-पीड़ित मुखिया भी छोटा बलिदान नहीं देता. वो अपने नवजात शिशु को उस दिव्य शिशु की रक्षा हेतु बलिदान की वेदी पर रख देता है और उस दिव्य शिशु के पालन और रक्षण का वचन देता है.
चूंकि समझने हैं प्रतीकार्थ
दोस्तों, श्रीकृष्ण के जन्म की कथा तो आप सबने हज़ारों बार सुनी होगी पर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ये कथा इन शब्दों में क्यों कही. चलिए अब खुलकर बात करते हैं. हम सब जानते हैं कि हमारे धर्मग्रंथों में सामान्य कथा के साथ प्रतीक कथाएं भी चल रही होती हैं. लेकिन श्रीकृष्ण का तो जन्म भी अपने आप में प्रतीक-अर्थ रखता है. कैसे? आइए इसे दो उदाहरणो से समझें.
पहला- कार्ल-मार्क्स, जिनके सिद्धांत अब पूरे विश्व में मान्य हो चुके हैं; उनका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या कहता है? जब अन्याय और शोषण इतना बढ़ जाता है कि जीवन जीने लायक नहीं रहता तो उस पीड़ित मानवता अर्थात् ‘सर्वहारा’ वर्ग में ही पूंजीपति या सत्ता को अपदस्थ करने के उस ‘संकल्प’ का जन्म होता है, जो क्रांति का अग्रदूत बनता है.
दूसरा– उस दंत कथा के माध्यम से जो ऊपर सुनाई गई है. जो हमें समझाती है कि जिन रस्सियों के कारण हम बंधा हुआ महसूस करते हैं, उनमें से अधिकांश का अस्तित्त्व केवल हमारे मन में है और उन्हें खोलने के लिए केवल आत्मबल और दृढ़ इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है.
श्रीकृष्ण का जन्म प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि मानव तभी निर्भय और निर्द्वन्द्व हो सकता है जब अपने भीतर स्थित ब्रह्म को पहचाने. तभी उसकी आत्मशक्ति का पूर्ण विकास होता है. उस दिन के बाद से मोह या भय के बंधन मिथ्या लगने लगते हैं. जब मानस में ज्ञान का आगमन होता है तो पूर्वाग्रहों की बेड़ियां ख़ुद ही टूट जाती हैं. विवेक के प्रस्फुटन से निराशा के पहरे हट जाते हैं. चेतना का संचार मानवता के मन में सुंदर भविष्य के रक्षण का उत्साह जगाता है. मानव उसके लिए कोई भी उत्सर्ग करने को तत्पर हो जाता है. इस प्रकार जन्मे सत-संकल्प की पूर्ति और रक्षण के लिए सम्पूर्ण प्रकृति और मानवता उसे स्वयं मार्ग देने लगती है.
सत्-संकल्पों का दिव्य शिशु
मध्य रात्रि का समय वो होता है, जब अंधकार अपने चरम पर होता है. अर्थात् मार्क्स के अनुसार अन्याय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका होता है और जीवन जीने लायक नहीं बचा होता है. बादल का गरजना, बिजली चमकना तमाम बेड़ियां और पहरे सामान्य जनता में व्याप्त भय और त्रास का प्रतीक हैं. मानव सभ्यता में अक्सर वो युग आता रहता है, जब शोषण की अधिकता और शासन के अतिशयता के साथ बढ़ गए दमनकारी दर्प से समाज ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता. जन सामान्य में ये भय व्याप्त हो जाता है कि शासन के ख़िलाफ़ बोलने वाला या किसी भी प्रकार शासन में अपने पतन का भय पैदा करने वाला कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक विरोध या आंदोलन कुचल ही दिया जाएगा. ऐसे में समाज के सामान्य और अशिक्षित वर्ग ही नहीं बुद्धिजीवी भी उस ऊंट की तरह हो जाते हैं. जिनके गले में निराशा की रस्सी है. उस पीड़ित जोड़े की बेड़ियां उसी भय या पूर्वाग्रह की प्रतीक हैं, जो कहती है कि कुछ नहीं होने वाला. ताले प्रतीक हैं उन तर्कों का, जो कहते हैं कि हमारे अकेले के विरोध से क्या हो जाएगा. प्रहरी प्रतीक हैं सत्ता द्वारा फैलाए गए दमनकारी उदाहरणों और समाचारों का, जो डराते हैं कि अगर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उस नवजात विचार, विरोध या आंदोलन का सिर पत्थर पर पटक दिया जाएगा, अगर किसी ‘ज्योतिषी’ ने बता दिया अर्थात् जिसकी गतिविधियों से सत्ता को अपने लिए ख़तरा लगा तो उसे कारागृह में डलवा दिया जाएगा, उसका जीवन यातना का पर्याय बना दिया जाएगा, उसके वंश की हत्या कर दी जाएगी.
और तब किसी पीड़ित बुद्धिजीवी को लगने लगता है कि बस, अब और नहीं. इस दमनकारी नीति का दमन करना ही होगा. फिर वेदना के गर्भ में विचार पलते हैं, पकते हैं और सत्-संकल्प के दिव्य शिशु के रूप में जन्म लेते हैं. इस दिव्य शिशु अर्थात् दमनकारी के विनाश के लिए जीवन समर्पित कर देने के संकल्प के जन्म लेते ही इनसान भय-मुक्त हो जाता है. वो सोच लेता है कि जीने लायक न बचे जीवन को जीने का क्या फ़ायदा? अगर जीना है तो इनसान की तरह, आत्मसम्मान के साथ, अपने उत्थान के लिए किए गए श्रम की सफलता के सपनो के साथ, भय-मुक्त और आनंद-युक्त होकर अन्यथा मर जाना है. संकल्प के इस दिव्य शिशु के जन्म के साथ ही भय की बेड़ियां कट जाती हैं, पूर्वाग्रह के ताले खुल जाते हैं, स्वार्थी तर्कों के प्रहरी सो जाते हैं और संघर्ष की राह दृष्टव्य होती जाती है.
इस संकल्प की रक्षा के लिए जब व्यक्ति हर त्याग करने को तत्पर हो जाता है तो गोकुल के मुखिया नंद की तरह पूरा पीड़ित समूह उसके साथ खड़ा हो जाता है. उसकी सफलता के लिए, उसके संकल्प की रक्षा करने और उसका पालन-पोषण कर उसे परिपक्व बनाने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार हो जाता है.
कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही जैसे कोई सीख है
श्रीकृष्ण को शायद इसीलिए जगतगुरु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस जग को संघर्षों में जी कर दिखलाया और जीना सिखलाया. उनके जन्म ने सिखाया कि जिस दिन मानव अपने भीतर स्थित ब्रह्म को पहचानने में सफल हो जाता है, मानव-निर्मित सभी बेड़ियां और पहरे उसके लिए मूल्यहीन हो जाते हैं. बचपन की चोरियों और अठखेलियों ने सिखाया कि घी, दूध मक्खन पर किसी अत्याचारी राजा का नहीं उसके उत्पादक ग्रामीणों का अधिकार है. और अधिकार कभी संघर्ष के बिना नहीं मिलते. कैशोर्य की बंसी और रासलीला ने सिखाया कि सम्पूर्ण त्रासदियों और विवशताओं के मध्य जीवन के माधुर्य को भी जीना चाहिए. तनाव-रहित तथा प्रेममय जीवन ही समाधान ढूंढ पाता है. युवावस्था की जरासंध तथा कालयवन की युक्तिपूर्ण हत्या ने सिखाया कि राजनीति का मतलब है स्वयं पर लांछन लगने की परवाह न करते हुए प्रजा की समृद्धि और सुरक्षा के युक्तिपूर्ण उपाय ढूंढ़ना. और प्रौढ़ावस्था ने कर्म और पौरुष का वो सिद्धांत दिया, जो आज विश्व में गीता के रूप में प्रसिद्ध है.
जन्माष्टमी पर पूजा और समारोह करना तो केवल माध्यम है उनकी शिक्षाओं को याद करने का. भक्ति का मतलब तो है नेक काम के लिए ख़ुद पर लांछन भी स्वीकार करने को तैयार रहना. आज बहुत से ऐसे बहुत से आंदोलनकारी हैं, जो समाजसेवी संगठन बनाकर या अकेले ही युग की किसी एक समस्या के साथ लड़ रहे हैं. अपनी संपूर्ण बुद्धि के साथ योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे हैं. बिना इस बात की परवाह किए कि वह क्या और कितना कर पाएंगे. वास्तव में केवल वही सच्चे कृष्ण भक्त हैं जो उनके जीवन-दर्शन को आत्मसात कर, युग की समस्याओं में पूर्णतः लिप्त हैं. समाधान के लिए प्रयत्नरत हैं.
फ़ोटो : फ्रीपिक