क्या आपने ग़ौर किया कि पिछले कुछ समय में इंटरनेट ने भले ही हमें जानकारियों के समंदर के बीच ला खड़ा किया हो, लेकिन बावजूद इसके हमारे अंदर दूसरों को ‘जज’ करने, ईर्ष्या करने, प्रतिद्वंद्विता करने, स्वतंत्रता के नाम पर मनमाना करने की आदत बढ़ी है. मतभेद बढ़े हैं. ज्ञान तो हर जगह फैला हुआ है, बावजूद इसके हमारी सोच संकुचित हुई है. फिर भला ऐसे ज्ञान का क्या उपयोग, जो माहौल को ज़हरीला बनाए और हमें खुल कर सांस भी न लेने दे? इसी बात पर है कनुप्रिया का यह नज़रिया.
देश मे ज़रा-ज़रा वैचारिक मतभेदों को लेकर फ़िल्मों का बायकॉट जारी है. अब सुना कि अपकमिंग फ़िल्म लाइगर के बायकॉट का सिलसिला भी चल पड़ा है, क्योंकि उसके लीड एक्टर ने आमिर ख़ान की लाल सिंह चड्ढा की तारीफ़ कर दी है. सोचती हूं कि हम दिन ब दिन किस कदर एक बेहद संकुचित मानासिकता की भेड़ चाल वाली भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं, जहां सोचना समझना गुनाह है, उदारता देशद्रोह है, राष्ट्रवाद का मतलब बस एक ही विचारधारा है.
आज की तरह हमारे बचपन मे एक क्लिक पर दुनिया उपलब्ध नहीं थी. आज ओटीटी प्लैटफ़ॉर्म ने घर बैठे दुनिया भर की फ़िल्मों से परिचित होने का मौक़ा दे दिया है, इंटरनेट हमे दुनिया मे कहीं भी जानकारी दे सकता है. इतनी सूचना ने भी अगर हमारे दिमाग़ के दरवाज़े-खिड़कियां नहीं खोलीं, तो साफ़ है कि महज़ सूचना और जानकारी की उपलब्धि आपकी समझ को मांझने की क्षमाता नहीं रखतीं, समझ की दिशा महत्वपूर्ण है.
अगर अपने बचपन में लौटूं तो दुनिया को जानने समझने का तरीक़ा हमारा बस प्रिंट लिटरेचर था. उसी लिखे और चित्रों के सहारे हमने दुनिया की कल्पना की, जिसमें विभिन्नताएं तो थीं, मगर द्वेष नहीं था.
दुनिया के अलग अलग देशों की लोक कथाएं हमारे बचपन का हिस्सा थीं. रूसी साहित्य तो आराम से मिल ही जाता था, सोवियत भारत मैत्री युग में. चीनी साहित्य भी घर में मिल गया था, अपने चाचा की वहां पोस्टिंग के कारण. उसके अलावा भी किताबों, अमर चित्रकथाओं, इंद्रजाल कॉमिक्स ने हमारी कल्पनाओं को और जानकारी को अच्छी भली उड़ान दी. चंदामामा से ही हमने विक्रम वेताल और अलिफ़ लैला को जाना, दुनियाभर की कहानियां मिलती थीं उसमें. जानकारी के स्रोत सीमित थे, मगर उसने हमारी मानसिकता को विस्तृत करने का ही काम किया.
कुछ ऐसा ही हाल संगीत का है, वो सरहद की सीमाओं को तोड़कर बहता है, वो वाक़ई विश्व को एक कुटुंब बनाने की क्षमता रखता है. आप सुनना शुरु करते हो तो इंग्लिश, कोरियन, स्पेनिश, मिस्र, अरब कहीं का संगीत ऐसा नहीं, जो आपको छूता नहीं. न उसके पीछे नस्ल दिखती है, न धर्म, न राष्ट्रीयता, न रंग, संगीत महत्वपूर्ण हो जाता है.
संगीत, लिटरेचर और खेल दुनिया को जोड़ते हैं, राजनीति तोड़ती है.
आज सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी को रबाब पर जन गण मन बजाते सुना, और याद आया कि कैसे हमारे देश मे लोग आपस में ही इसपर लड़ रहे थे कि सिनेमा हॉल में कौन खड़ा होता है, कौन नहीं! क्या इससे साबित होगा कौन देशभक्त है?
भारत की सबसे बड़ी प्रसिद्धि इसी में थी कि यहां सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता के लोग भी आपस मे एक राष्ट्र के रूप में मिलकर रहते हैं इसीलिए तो हम विश्व गुरु थे. आज उदारता का ये हाल है कि हम एक विशेष विचारधारा से विपरीत कुछ बोलते ही ख़ुद अपने देश के द्रोही हो जाते हैं, विश्व तो छोड़ ही दो. घर मे एक दूसरे का गला काटने को तत्पर लोग जब विश्व मंचों पर ख़ुद को विश्व गुरु कहते हैं तो ‘लानत है’ कहने का मन होता है.
क्या हम वाक़ई इतनी ही संकुचित मानसिकता के थे और उदारवादी पार्टियों (तथाकथित) की सत्ता के चलते हमारी संकुचित मानसिकता ढंकी छुपी थी? या अब एक ही रंग, एक ही धर्म की संकुचित विचारधारा वाली पार्टी, जिसने ख़ुद को “राष्ट्रवादी” पार्टी जैसा महत नाम अपनी तंगनज़री को छुपाने के लिए दिया है, उसकी सत्ता के आते ही असल भारतीय मानसिकता उजागर हो गई कि हमारे नाम बड़े हैं, मगर दर्शन छोटे ही हैं, या फिर इस राज में लोगों को दिन ब दिन एक योजनाबद्ध तरीक़े से संकुचित बनाया जा रहा है कि असहमति शब्द से ही असहमति हो गई है. बकौल जार्ज बुश, या तो आप दोस्त हैं या दुश्मन.
जो भी है, हमेशा बन्द कमरों में रहने वालों को जैसे उसी की आदत हो जाती है, खुली हवा का महत्व पता नहीं चलता, वही हाल फ़िलहाल देश की हवा का है.
काश! खुली सांस के दिन फिर से लौटें.
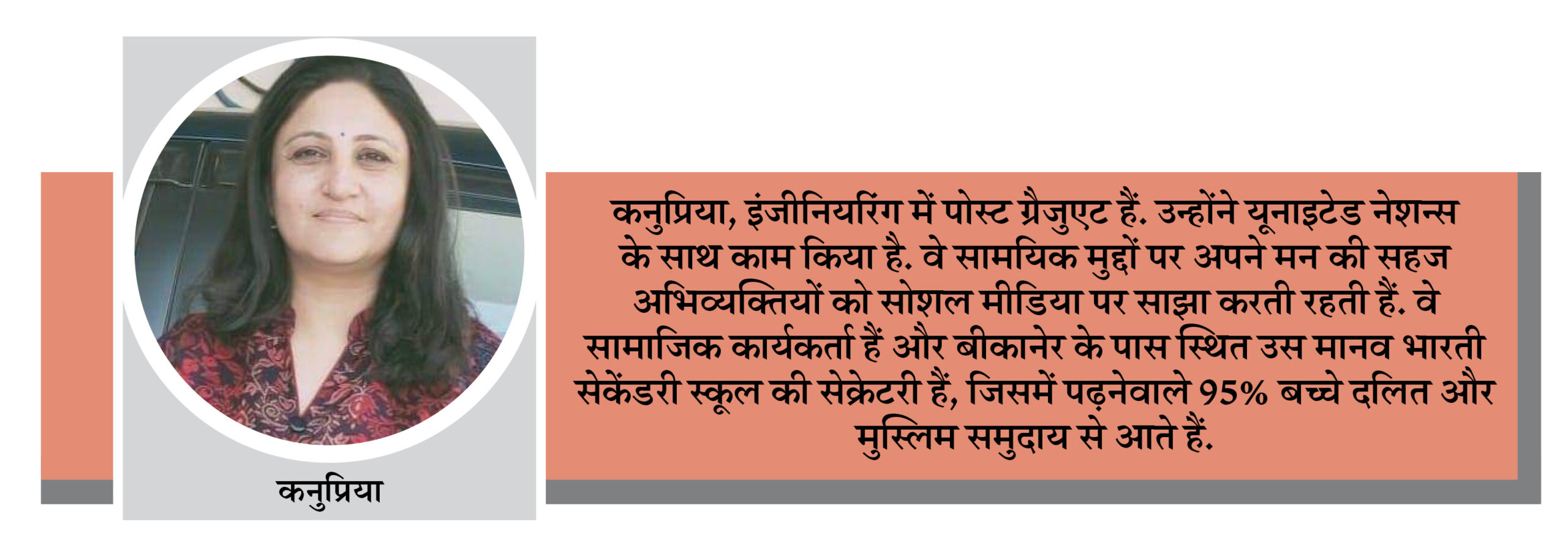
फ़ोटो: पिन्टरेस्ट, themindsjournal.com









